डिग्रियों की दौड़ में दम तोड़ते सपने_संभावनाओं की कब्रगाह बनते संस्थान
*संस्थाएं डिग्रियां नहीं, ज़िंदगियां दें — तभी शिक्षा का अर्थ है*
भारत में शिक्षा संस्थान अब केवल डिग्रियों की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं, जहां बच्चों की संभावनाएं और संवेदनाएं दोनों दम तोड़ रही हैं। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहर आत्महत्या के आंकड़ों से दहल रहे हैं।
यह संकट केवल परीक्षा का नहीं, हमारी सोच और व्यवस्था का है — जो रैंक को जीवन से ऊपर रखती है। शिक्षा में संवाद, मानसिक परामर्श और मानवीयता की जगह खाली है।
जब तक हम शिक्षा को जीवन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह व्यवस्था सफल नहीं, घातक सिद्ध होती रहेगी।
प्रियंका सौरभ
कभी जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों को ज्ञान के मंदिर कहा जाता था, आज वही स्थान धीरे-धीरे उस पीड़ा के पर्याय बनते जा रहे हैं।
जहां बच्चों की हँसी नहीं, तनाव भरी चुप्पी गूंजती है। एक दौर था जब शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुंदर बनाना था, आज शिक्षा जीवन का भार बन गई है।
हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां विद्यार्थी शिक्षा से नहीं, शिक्षा के ढांचे से डरने लगे हैं।
कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे — न जाने कितने शहरों में हर साल सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। ये केवल घटनाएं नहीं हैं, ये हमारे तंत्र की हार की घोषणा हैं।
राजस्थान का कोटा शहर, जिसे आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का केंद्र माना जाता है, वह इस समय देश का सबसे बड़ा मानसिक तनाव केंद्र भी बनता जा रहा है।
हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी या वैज्ञानिक बनने के सपने लेकर यहां आते हैं। लेकिन इन सपनों की कीमत इतनी भारी होती है कि सैकड़ों बच्चे उस बोझ को सह नहीं पाते और जीवन समाप्त कर बैठते हैं।
कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई अब एक मानसिक परीक्षा बन चुकी है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कक्षाएं, गृहकार्य, परीक्षा, फिर परिणाम — इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई द्वार नहीं होता।
विद्यार्थियों के लिए न तो खेल-कूद का समय होता है, न साहित्य, संगीत या संवाद का। न दोस्तों के लिए समय होता है, न अपने आप से बात करने का।
ऐसे माहौल में जब कोई बच्चा असफल होता है, तो वह स्वयं को जीवन के अयोग्य समझ लेता है।
यह मानसिकता इतनी गहरी है कि वह सोच भी नहीं पाता कि जीवन केवल एक परीक्षा से तय नहीं होता।
एक छात्र की आत्महत्या केवल एक जीवन का अंत नहीं है, वह उस शिक्षा व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी है जो विद्यार्थियों को नंबर और रैंक के तराजू में तौलती है।
यह भी पढ़ें
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार 2021 में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। यह संख्या भारत में शिक्षा के नाम पर होने वाली त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है।
क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की कि ये बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या केवल परीक्षा में असफल हो जाना किसी को जीवन त्यागने के लिए मजबूर कर सकता है?
दरअसल, समस्या परीक्षा की नहीं है, समस्या उस सोच की है जिसमें असफलता को कलंक माना जाता है।
माता-पिता, समाज, शिक्षक, कोचिंग संस्थान — सब इस मानसिकता को पोषित करते हैं कि जो बच्चा प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ, वह निकम्मा है।
परिणामस्वरूप, बच्चा स्वयं को दोषी मानने लगता है और धीरे-धीरे अवसाद की गर्त में चला जाता है। किसी से अपनी बात कहने का साहस भी उसमें नहीं रहता।
भारत की शिक्षा प्रणाली में वर्षों से यह कमी रही है कि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई।
विद्यालयों और महाविद्यालयों में न तो स्थायी मानसिक परामर्शदाता होते हैं, न छात्रों के साथ खुला संवाद।
माता-पिता भी अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा क्या महसूस कर रहा है। बच्चों से ‘कैसे हो’ पूछने के बजाय ‘कितना पढ़ा’ पूछा जाता है।
शिक्षा व्यवस्था की इस अमानवीयता को और अधिक तीव्र बना दिया है शिक्षा के व्यावसायीकरण ने।
आज शिक्षा एक सेवा नहीं, एक उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थान करोड़ों का व्यापार करते हैं।
उनका उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा में सफल बनाना है, उन्हें जीवन में सक्षम बनाना नहीं।
वे बच्चों को उत्तर याद करवाते हैं, सवाल पूछने की आदत नहीं सिखाते। वे सफलता की मशीनें गढ़ते हैं, इंसान नहीं।
बात केवल कोचिंग की नहीं है। देश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से भी आत्महत्याओं की खबरें आती रही हैं।
रोहित वेमुला, एक शोधार्थी, जिसकी आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था, वह भी संस्थागत भेदभाव और असंवेदनशीलता का शिकार था।
आज भी जातीय, सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव के अनेक रूप हमारे शैक्षिक संस्थानों में मौजूद हैं।
विद्यार्थियों को मानसिक सुरक्षा नहीं मिलती, भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वे जीवन को ही समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।
समस्या बहुत गहरी है और इसका समाधान केवल “शोक प्रकट करने” या “नियमन बनाने” से नहीं होगा। हमें शिक्षा की परिभाषा को फिर से गढ़ना होगा।
शिक्षा केवल डिग्री, अंक या नौकरी का माध्यम नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को समझना, आत्मविश्वास विकसित करना, और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक शिक्षा संस्थान में स्थायी मानसिक परामर्शदाता हों।
बच्चों के लिए खुला मंच हो जहां वे अपने विचार, भावनाएं और समस्याएं बिना डर के व्यक्त कर सकें।
परीक्षा पद्धति ऐसी हो जो केवल रटंत विद्या को न परखे, बल्कि रचनात्मकता, तर्कशक्ति और संवेदना को भी महत्व दे।
इसके साथ ही, कोचिंग संस्थानों पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है।
उनकी फीस, समय-सारणी, परीक्षा पद्धति — सब कुछ सरकार द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत लाना होगा।
सरकार को भी इस विषय पर केवल बयानबाज़ी करने के बजाय ठोस नीति बनानी चाहिए जो आत्महत्याओं की घटनाओं को रोक सके।
माता-पिता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। बच्चों से संवाद बढ़ाना होगा, उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी असफलता कोई अपराध नहीं है।
हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, और हर किसी की सफलता की परिभाषा एक जैसी नहीं हो सकती।
यह भी आवश्यक है कि समाज में असफलता को सहजता से स्वीकार करने की संस्कृति विकसित की जाए। हमें यह सिखाना होगा कि परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है।
यदि कोई बच्चा एक परीक्षा में नहीं सफल हो पाया, तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। यह जीवन केवल रैंक की सूची नहीं है, यह भावनाओं, संवेदनाओं और संभावनाओं की यात्रा है।
हमारा देश तभी शिक्षित माना जाएगा जब यहां के शिक्षा संस्थान बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं, जीवन जीने की कला सिखाएं। जब विद्यार्थी केवल डिग्रियां नहीं, उद्देश्य लेकर निकलें। जब शिक्षा बच्चों को नंबरों से नहीं, उनकी पहचान से जोड़ें।
आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम बच्चों को “किताबें रटवाएं”, बल्कि इस बात की है कि हम उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देना सीखें।
उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे जैसे हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं। उनकी संभावनाएं अंकतालिकाओं से बड़ी हैं, और उनका जीवन परीक्षा के परिणामों से अधिक मूल्यवान है।
अगर हम यह नहीं कर सके, तो हर वर्ष हजारों रोशनी बुझती रहेंगी, और हम केवल मोमबत्तियां जलाकर अफ़सोस करते रहेंगे।
शिक्षा को फिर से जीवनमूल्य आधारित बनाना होगा — जहां विद्यार्थी केवल डिग्री नहीं, उद्देश्य पाएं; केवल नौकरी नहीं, पहचान पाएं; और केवल पढ़ाई नहीं, जीने का विश्वास पाएं।
सम्बन्धित ख़बर यह भी पढ़ें






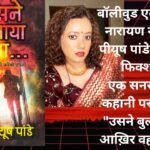


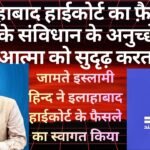


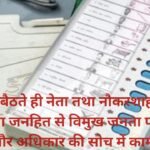








No Comments: